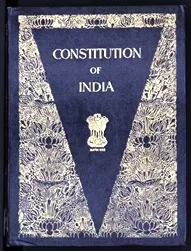
भारतीय संविधान के पचहत्तर साल पूरे होने के अवसर पर तमाम पूंजीवादी पार्टियों ने संसद में इस पर बहस की। इस अवसर पर उन्होंने इस संविधान के रूप और अंतर्वस्तु पर चर्चा करने के बदले अपना सारा ध्यान एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप पर लगाया। खासकर कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया। भाजपा ने अतीत पर ध्यान केंद्रित किया तो कांग्रेस ने वर्तमान पर। कहना मुश्किल है कि इस द्वंद युद्ध में किसने दूसरे को ज्यादा चोट पहुंचाई।
इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 75 सालों में सभी पूंजीवादी पार्टियों ने संविधान की ऐसी-तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केवल एक उदाहरण के तौर पर धारा 370 को लिया जा सकता है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सभी ने धारा-370 की मूल भावना का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर को उधर धकेला जिधर खुले विद्रोह और फिर आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं होना था। अंत में नरेंद्र मोदी की भाजपा ने और भी नंगेपन से स्वयं इस धारा को ही बदल दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने और भी नंगे ढंग से इस असंवैधानिक कृत्य पर मुहर लगा दी। यह एक उदाहरण यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने संविधान के शब्दों और भावना के साथ कैसे खिलवाड़ किया है। यह उदाहरण यह भी दिखाता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कैसे इस सबमें बराबर का भागीदार रहा है। स्वयं को संविधान का रक्षक घोषित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इसका उल्लंघन करता रहा है या उल्लंघन होने देते रहा है।
लेकिन शासक पूंजीवादी पार्टियों द्वारा इस संविधान के उल्लंघन से इतर दो ज्यादा बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि यदि यह उल्लंघन नहीं होता तो क्या होता? दूसरा यह है कि यह उल्लंघन होता क्यों रहा है?
शासक वर्ग के बुद्धिजीवियों की ओर से अक्सर इस किस्म की बातें आती हैं कि यदि भारतीय संविधान को उसकी भावना में लागू किया गया होता तो आज इसकी तस्वीर कुछ और ही होती। क्या वास्तव में ऐसा था?
कोई भी संविधान किसी समाज का एक अमूर्त प्रतिबिम्ब होता है जो साथ ही इस समाज के सीमित स्तर के परिवर्तन को अपने भीतर समेटे होता है। इसीलिए कोई भी संविधान किसी समाज के लिए तभी तक मौजूं होता है जब तक कि वह समाज मोटा-मोटी वही होता है। समाज में कोई बड़ा परिवर्तन होते ही उस समाज को एक नए संविधान की जरूरत होने लगती है। संवैधानिक संशोधनों से तभी तक काम चल सकता है जब तक समाज उसी दायरे में रहता है। एक-दो उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1788 में लागू हुआ। तब से वह बहुत थोड़े से संशोधनों के साथ चल रहा है। इसकी वजह यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज का निर्माण पूर्णतया पूंजीवाद के आधार पर हुआ। यूरोप से वहां जाकर बसे लोगों ने इसका निर्माण किया था। ये अप्रवासी अपने मूल समाज के सामंती अवशेषों को पीछे छोड़ आए थे। अमेरिका तब से आज तक इसी पूंजीवादी आधार पर आगे विकसित होता रहा है। इसीलिए अमरीकी संविधान इस समाज की जरूरतों को पूरा करता रहा है। पूंजीवादी दायरे में इस समाज में होने वाले परिवर्तनों को संविधान में संशोधन के जरिए समाहित किया जाता रहा है।
इसके बरक्स फ्रांस है। फ्रांस में 1789 की क्रांति से लेकर आज तक कई संविधान बने और निरस्त हुए हैं। स्वयं 1789-99 के क्रांति काल में ही तीन-चार संविधान बने और निरस्त हुए। आज फ्रांस के गणतंत्र को पांचवा गणतंत्र कहा जाता है। इन पांचों गणतंत्रों के अलग-अलग संविधान रहे हैं। बीच के गैर-गणतंत्रीय कालों के अपने संविधान थे। फ्रांस के इतने सारे संविधानों की क्या वजह हो सकती है? यही कि फ्रांस करीब 200 सालों तक लगातार उथल-पुथल का शिकार रहा है। पुराने सामंती समाज की जकड़न से मुक्त होने में उसे 100 साल लग गए और इसके लिए चार क्रांतियों की आवश्यकता हुई। उसके बाद भी समाज स्थिर नहीं हो पाया। केवल 1968 के बाद के काल को ही अपेक्षाकृत स्थिरता का काल माना जा सकता है।
1947-50 का भारत एक बहुत ही उलझा हुआ जटिलताओं भरा समाज था। सामाजिक व्यवस्था के तौर पर यहां कबीलाई, सामंती, पूंजीवादी सारे समाज थे। अति आधुनिक मुंबई-दिल्ली से लेकर आदिम अंडमान-निकोबार तक सब इसमें थे। यहां भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों की भरमार थी। अंग्रेजों ने रेल, डाक तार से पूरे भारत को प्रशासनिक तौर पर एक सूत्र में बांध दिया था पर भारत वास्तव में एक नहीं था। ऊपर से वर्ण-जाति व्यवस्था का नासूर समाज के पोर-पोर में व्याप्त था।
भारतीय समाज के निर्माता स्वयं इस समाज की पैदाइश थे। एक तो भारत की यह विविधता और जटिलता स्वयं संविधान सभा में विभिन्न व्यक्तियों के रूप में अभिव्यक्त हो रही थी। दूसरे, इन सारे लोगों को मिलाकर इसे संविधान में अभिव्यक्त करना था। अक्सर भारत के संविधान के बहुत बड़ा होने तथा ढेरों देशों के संविधान से उधार लेने की बात होती है। पर एक रूप में देखा जाए तो संविधान निर्माताओं के सामने और कोई रास्ता नहीं था।
1947-50 का भारतीय समाज किसी पूंजीवादी क्रांति के जरिये अस्तित्व में नहीं आया था कि इसमें अतीत के झाड़-झंखाड़ को उखाड़ कर नष्ट कर दिया गया हो। तब भारतीय समाज ज्यादा एकरस होता और उसके आगे की गति ज्यादा सम होती। पर ऐसा नहीं था और संविधान निर्माताओं का किसी क्रांतिकारी बदलाव का इरादा भी नहीं था। वे क्रमिक सुधारों के जरिए भारतीय समाज के क्रांतिकारी रूपान्तरण के पक्षधर थे।
इन सबके कारण भारत का संविधान एक अजीब सी खिचड़ी बन गया। यह संविधान निजी सम्पत्ति की रक्षा करता था तथा कुल मिलाकर इसकी दिशा पूंजीवादी थी। पर इन दो के अलावा बाकी सारा कुछ अनिश्चित था। और स्वयं संविधान बनाने वालों ने इसे भांति-भांति से स्वीकार किया। अम्बेडकर ने कहा कि आगे क्या होता है वह इस पर निर्भर करेगा कि संविधान को लागू करने वाले कैसे लोग होंगे। यानी संवैधानिक संस्थाओं के बदले सारा कुछ व्यक्तियों पर निर्भर होना था। इसी तरह धर्म निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को अपरिभाषित छोड़ दिया गया। सामाजिक रूपान्तरण के ढेर सारे उपायों को नीति निर्देशक सिद्धान्तों की सूची में डालकर व्यवहार में इनके लागू होने को लोगों की इच्छाओं के हवाले कर दिया गया। स्वयं मूलभूत अधिकारों को भी इस शब्दावली में तथा इतने सारे किन्तु-परन्तु के साथ परिभाषित किया गया कि इनकी कोई भी व्याख्या की जा सकती थी।
इस तरह देखा जाये तो जब लोग यह कहते हैं कि यदि संविधान को उसकी मूल भावना में लागू किया गया होता तो देश की तस्वीर कुछ और होती तो यह बातें एकदम बेमानी हैं। असल में निजी सम्पत्ति की रक्षा और पूंजीवादी दिशा के अलावा इसकी कोई मूल भावना है ही नहीं। इसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे के अपने प्रसिद्ध फैसले में रेखांकित किया।
अब यदि संविधान की मूल भावना निजी सम्पत्ति की रक्षा और पूंजीवादी दिशा थी तो इससे अंततः कौन सा भारत बनता? वही जो बना। बहुत सारे लोगों को आज रंज है कि पश्चिमी देशों जैसा विकसित पूंजीवादी देश बनने से तो भारत कोसों दूर है ही, यह चीन जैसे देश से भी बहुत पीछे छूट गया है। पर ये सारे लोग यह भूल जाते हैं कि चीन ने पचहत्तर साल पहले अपने विकास की यात्रा की शुरूआत एक बेहद आमूलगामी क्रांति से की थी। भारत के शासकों ने ठीक इसी तरह की क्रांति से बचने का हर संभव प्रयास किया। यहां तक कि वे किसी आमूलगामी सुधार से भी बचे। परिणामस्वरूप भारतीय समाज अतीत के सारे कूड़े-करकट के बोझ से लदा रहा। अतीत का इतना सारा बोझ सिर पर लादकर वह पूंजीवादी विकास के रास्ते पर सरपट नहीं दौड़ सकता था।
इसलिए यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यदि भारतीय संविधान को सही तरीके से उसकी भूल भावना में लागू किया गया होता तो उसकी तस्वीर कुछ और होती। असल में आज भारत जो कुछ है, वह उसी संविधान का परिणाम है। उन्नीस-बीस की गुंजाइश के साथ इससे भिन्न नहीं हो सकता था।
तो क्या आज के भारत में ऐसा होने में व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं थी? क्या पूंजीवादी पार्टियां और पूंजीवादी नेता निर्दोष हैं? क्या सारा जिम्मा इतिहास की निर्वैयक्तिक शक्तियों का है?
बात इसके ठीक उलट है। जैसा कि पहले कहा गया है। भारत के संविधान की संरचना ही इस रूप में बनाई गयी कि इसमें संस्थाओं के बदले व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जानी थी। यानी संविधान द्वारा निर्देशित समाज की गति संविधान द्वारा गठित संस्थाओं के बदले इन संस्थाओं पर काबिज व्यक्तियों पर निर्भर होनी थी। यदि आज हिन्दू फासीवादी नेहरू बनाम पटेल का मुद्दा उठाते रहते हैं तो उसमें यह बात अंतर्निहित होती है कि यदि नेहरू के बदले पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भारत 1947 से ही हिन्दू साम्प्रदायिक रास्ते पर चल पड़ा होता। स्वयं अम्बेडकर के कथनानुसार इस निष्कर्ष की पर्याप्त गुंजाइश है।
जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय संविधान द्वारा संस्थाओं के बदले व्यक्तियों की इस भूमिका की गुंजाइश बनाने का काम भारत की जटिलताओं के मद्देनजर किया गया था। यह वह लचीलापन था जिससे भारत की जटिलताओं से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने की उम्मीद की गयी थी। इस उम्मीद में नेताओं की सदिच्छा की कल्पना कर ली गयी थी।
लेकिन वर्गों-तबकों में विभाजित अन्याय-अत्याचार और शोषण वाले समाज में नेताओं की सदिच्छा का क्या मतलब हो सकता था? बहुत छूट देकर बात की जाये तो अच्छा से अच्छा पूंजीवादी नेता भी केवल यही कर सकता है कि वह व्यक्तिगत और अपने वर्ग-तबके के हितों के साथ पूरे समाज के हितों का भी ख्याल रखे। पर पूरे समाज का हित किसमें है यह पहले से निश्चित नहीं होता। यह व्यक्ति की अपनी वर्गीय-तबकाई दृष्टि से तय होता है जिसमें उसके अपने व्यक्तिगत हितों की भी भूमिका होती है। इसीलिए पूरे समाज के हित का अर्थ नेहरू, पटेल, अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए अलग-अलग था। वे उसी संविधान की अलग-अलग दिशा देखते थे जिसे उन्होंने सामूहिक तौर पर बनाया था। इसीलिए सत्ता के शीर्ष पर इनके होने से समाज की दिशा अलग-अलग होनी थी। और चूंकि संविधान की संरचना ही इस बात की इजाजत देती थी कि समाज की दिशा के निर्धारण में संस्थाओं के शीर्ष पर विद्यमान व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो, तो यह महत्वपूर्ण हो ही जाता था कि शीर्ष पर कौन व्यक्ति विद्यमान है।
इसी से इस बात का भी जवाब मिलता है कि भारतीय संविधान का उल्लंघन क्यों होता रहा है। जिस हद तक संविधान स्वयं धारा-352, 54 व 56 (आपातकाल) तथा धारा-368 (संविधान संशोधन) के जरिये इसकी इजाजत देता रहा है, उस हद तक तकनीकी तौर पर इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसीलिए 1975-77 का आपातकाल तथा 1976 का 42वां संविधान संशोधन संविधान का तकनीकी तौर पर उल्लंघन नहीं थे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कभी असंवैधानिक ठहराया भी नहीं। पर तकनीकी तौर पर भले ही वे उल्लंघन न हों पर वास्तव में वे थे और मजे की बात यह है कि संविधान इसकी इजाजत देता था। यह उसी अंतर्विरोध का एक रूप था जिसका चरम यह है कि स्वयं संविधान के जरिये संविधान को निरस्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे के फैसले ने इसकी एक सीमा बांधी थी पर यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय बुनियादी ढांचे के अपने फैसले को ही बदल नहीं देगा। वास्तव में हिन्दू फासीवादी अपने हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। इसीलिए वे न्यायालयों में अपनी सोच के लोग भरती कराते जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे लोगों की भरमार हो जाने पर अपना मकसद पूरा करने में वे कामयाब हो जायेंगे। वे बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना हिन्दू राष्ट्र कायम कर लेंगे। धारा-370 व बाबरी मस्जिद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देखते हुए यह बहुत दूर की कौड़ी नहीं लगती।
भारतीय संविधान की और इसके द्वारा निर्मित व संचालित इस समाज की गति को देखते हुए उन लोगों की समझ पर ज्यादा से ज्यादा तरस ही खाया जा सकता है जो संविधान बचाने की कसम खाते हैं। इस संविधान को बचा कर उससे ज्यादा हासिल नहीं किया जा सकता जैसा आज समाज है। और इस समाज को एक अच्छा समाज तो ये लोग भी नहीं कहेंगे। समाज को और ज्यादा बदतर होने से बचाने में अपनी सारी ऊर्जा लगाना कहीं से भी बुद्धिमानी का काम नहीं है।
इसके बदले ठीक उल्टा करने की जरूरत है। समाज के क्रांतिकारी बदलाव की मुहिम ही समाज को और बदतर होने से रोक सकती है। क्रांतिकारी संघर्षों के उप-उत्पाद के तौर पर सुधार हासिल किये जा सकते हैं। और यह क्रांतिकारी संघर्ष संविधान बचाने के झंडे तले नहीं बल्कि ‘मजदूरों-किसानों के राज का नया संविधान’ बनाने के झंडे तले ही लड़ा जा सकता है जिसकी मूल भावना निजी सम्पत्ति का उन्मूलन और सामूहिक समाज की स्थापना होगी।
यह भी पढ़ें :-
1. संविधान की मूल भावना: निजी सम्पत्ति की रक्षा















