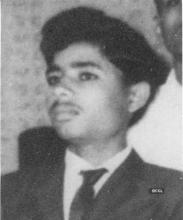देश में व्याप्त भयंकर बेरोजगारी तथा गरीबी व बदहाली के बावजूद मोदी सरकार करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर रही है। इनसे पहले की कांग्रेस सरकार ने भी रोजगार उपलब्ध कराने का वादा पूरा नहीं किया था। इससे भी पहले की वाजपेयी सरकार ने भी इस सम्बन्ध में वादा खिलाफी की थी। असल में देश की आजादी के बाद की सभी सरकारों ने इस मुद्दे पर कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है। एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगारी, गरीबी व बदहाली से, पीढ़ी दर पीढ़ी, छटछपाटे रहे और दूसरी तरफ सरकारें देश के विकास, अर्थव्यवस्था में सुधार और जीडीपी में वृद्धि दर आदि जैसी बातें करती रहीं और यही बातें आज भी हो रही हैं। बेरोजगारों को कुछ फौरी राहत देने का जिक्र भी नहीं हो रहा। लेकिन हजारों करोड़ रुपया अर्थव्यवस्था में ‘गति’ लाने के लिए झोंक देने की बातें जरूर शुरू हो गयी हैं। इसके लिए बजट घाटा बढ़ा देने को भी सरकार तैयार दिख रही है। <br />
करोड़ों बेरोजगार अपनी जिन्दगी में कुछ उजाला लाने के लिए कोई काम ढूंढ रहे हैं और यह अवसर उन्हें नहीं मिल रहा है, वे निराशा में पड़े हैं पर सरकारें उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। वे ऐसा जानबूझ कर कर रही हैं। देश की आजादी के बाद जब देश की तरक्की के लिए योजना आयोग बना और पहली पंच वर्षीय योजना बनी तभी यह निर्धारित कर लिया गया था कि रोजगारों के सृजन का कोई लक्ष्य अलग से नहीं लिया जायेगा। योजना के अंतर्गत होने वाले विकास के नतीजों के रूप में ही रोजगार सृजन होगा। सरकार ने रोजगार सृजन सम्बन्धी कीन्स की अवधारणा को लागू करने से इंकार कर दिया था। इससे अलग मजदूरी स्तर को ऊंचा-नीचा कर समायोजन करते हुए लेबर मार्केट को क्लीयर करने के रास्ते को भी लागू करने से मना कर दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण-रोजगार को एक ऐसा लक्ष्य माना गया जो एक ‘‘लम्बे दौर’’ में, तेज विकास दर के परिणाम के रूप में, कभी हासिल हो सकेगा। यह भी कि देश के आगामी औद्योगीकरण की तकनीक भी पूरे तौर से श्रम सघन नहीं होगी। खासकर भारी उद्योगों में उच्च तकनीक की जगह श्रम सघन (जो अपेक्षाकृत ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है) इस्तेमाल करने की इजाजत कतई नहीं दी जायेगी। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में जरूर ही, उच्च तकनीक पर तुरन्त जोर नहीं दिया गया क्योंकि इससे मजदूरों की छंटनी हो जाती। इस सबके बावजूद यह नहीं माना गया कि बेरेाजगारी एक समस्या के रूप में है। योजनाओं के शुरूआती दौर में, इस सम्बन्ध में सरकार की पहुंच (Approach) ही यह थी कि ‘विकास’ के लिए श्रम का इस्तेमाल किया जाये न कि बेरोजगारी दूर करने के दृष्टिकोण से। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने अनुमान लगाया था कि लगभग 50 लाख लोग पहले से बेरोजगार हैं और 2 लाख प्रति वर्ष इसमें और शामिल हो रहे हैं पर तय किया गया कि रोजगार का सृजन विकास प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होगा। इसके लिए अलग से कुछ नहीं किया जायेगा। पर घोषणा की गयी कि अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और बेरोजगारों को काम मिलेगा। पर ऐसा न होना था और न ही हुआ। अर्थव्यवस्था, 60 व 70 के दशक में, मात्र 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी। रोजगारों का सृजन 2 प्रतिशत की दर से ही बढ़ा और इस दौर में श्रम शक्ति में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोत्तरी हुई। नतीजा 1956 में 50 लाख बेरोजगार बढ़ कर 1977-78 में एक करोड़ दस लाख तक पहुंच गये। (यह संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। बेरोजगारों की तादाद वास्तव में कहीं अधिक थी।) पांचवीं पंचवर्षीय योजना(1974-79) में रोजगार सृजन को एक ‘‘अति महत्वपूर्ण चुनौती’’ माना गया लेकिन फिर वही कि योजना में निहित ‘विकास’ के परिणामस्वरूप ही यह बेरोजगारी दूर होगी पर इतिहास है कि वह नहीं हुई। बेरोजगारी व बदहाली की त्रासदी अपने विभिन्न आयामों और विभिन्न प्रकार के विकास के साथ आज भी करोड़ों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाये हुए है और राहत की रोशनी दूर-दूर तक भी नहीं है। एक तरफ बेरोजगारी, बदहाली व भीषण गरीबी का यह अथाह समन्दर है और दूसरी ओर देश के उद्योगों के मालिकों-पूंजीपतियों-अरबपतियों के तबके में जबरदस्त उन्नति! सरकार के सभी प्रयासों का फल इन्हें ही मिला। आखिर सत्ता पूंजीपतियों के वर्ग की है। <br />
हालात यह हैं कि पूरे देश की आबादी- एक एक व्यक्ति का आधार बनवा लेने वाली सरकार का, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि ‘देश में बेरोजगारी के उपलब्ध आंकड़े निर्भर होने योग्य नहीं हैं’। सही है कि एक प्रकार से बेरोजगारों की उनकी गणना से बेरोजगारी 2 से 3 प्रतिशत है और दूसरी प्रकार से आंकलन किये जाने पर 5 से 8 प्रतिशत बतायी जाती है। क्या करे बेचारी सरकार! कोई भी जान सकता है कि सवाल आंकलन का नहीं बल्कि सरकार की नीयत और पक्षधरता का है। देश में पूंजीपतियों के मुनाफे के अतिरिक्त सभी सवाल प्रशासनिक सवाल हैं। <br />
इस सिलसिले में यह देखना और भी कष्टदायक होगा कि देश के आम बेरोजगारों को सरकार कैसा काम दिलाना चाहती है तथा बेरोजगार को यदि काम मिला तो उन्हें कितनी मजदूरी मिलेगी? दूसरे शब्दों में, देश का आम बेरोजगार, काम मिलने के बाद, यदि ‘गरीबी रेखा’ से ऊपर उठेगा तो कितना उठेगा? गैर गरीब भारतीयों की स्थिति, सरकार की नजर में, कैसी है? देश में जब योजनाबद्ध विकास की शुरूआत हो रही थी तभी सरकार ने यह मान लिया था कि देश में आर्थर लुइस(नोबल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री) का ‘सिद्धान्त’ लागू होगा ही। मोटे तौर पर लुइस का कहना है कि विकासशील देश में, जहां परम्परागत खेती-बाड़ी में बहुसंख्य आबादी लगी है तथा इनकी मजदूरी/आमदनी इतनी है कि केवल वे मात्र जिन्दा रह पा रहे हैं, इनमें से यदि लोगों को खेती-बाड़ी से हटा कर देश में ही मौजूद औद्योगिक/आधुनिक क्षेत्र में लगा दिया जाय और उनकी मजदूरी लगभग उतनी ही रहने दी जाये(मात्र जीने लायक- Subsistance wage) यानी मजदूरों की मजदूरी व उनका उपभोग स्तर न बढ़ने दिया जाये तो बिना किसी खास खर्च के देश के पूंजीपति वर्ग को मजदूर मिल जायेंगे- वे मुनाफा कमायेेंगे- मुनाफे को पुनः देश के उद्योगों में लगायेंगे और इस प्रकार देश का औद्योगीकरण बढ़ेगा तथा खेती-बाड़ी क्षेत्र से लोगों के हटने से खेती का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। लुइस बताते हैं कि इस प्रकार के देशों में आबादी के भयंकर रूप से बढ़ने से मजदूरों की आपूर्ति अत्यधिक हो गयी है और ये लोग किसी न किसी तरह खेती बाड़ी से चिपके हुए हैं- छिपी हुयी बेरोजगारी में जी रहे हैं। इन देशों में लाखों-करोड़ों लोग जूता पालिश करने, पल्लेदारी करने, चौकीदारी करने तथा होटल में बेटर बनने जैसे अस्थायी/अंशकालिक कामों में लगे हैं। जमींदारों-सामंतों के यहां भी इस तरह के लोगों की फौज लगी रहती है ताकि जमींदारों का रुतबा बना रहे। महिलाएं केवल घरेलू काम करते-करते अपनी जिन्दगी बिता रही हैं। इस तरह के लोग किसी प्रकार के ‘उत्पादन’ में नहीं लगे हैं जिन्हें स्थानान्तरित कर पूंजीपतियों के पास भेजकर खटाया जा सकता है। खास बात यह है कि कुल मिलाकर मजदूरी और उपभोग का स्तर न बढ़ने दिया जाये। मात्र 20-30 प्रतिशत ज्यादा मजदूरी यदि उद्योगों में/आधुनिक क्षेत्रों में मिलेगी तो इसी लालच में उक्त मजदूर स्थानान्तरित होने के लिए तैयार रहेंगे।<br />
ऐसा ही हुआ है और हो रहा है। दूर-दूर देहातों से मजदूर जब उद्योगों में/आधुनिक क्षेत्रों में आकर खटते हैं तो उन्हें वहां मिलता क्या है? लुइस के अनुसार, सरकार की नीयत के अनुसार उन्हें पहले ही अल्प मजदूरी से मात्र 20-30 प्रतिशत के लगभग ही बढ़ी मजदूरी अथवा सुविधाएं मिल पाती हैं। उनके जीवन स्तर/उपभोग स्तर में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं होता है। ‘गरीबी रेखा’ से ऊपर परन्तु गरीबी रेखा पर। <br />
सरकारों में बैठे नेता लोग या बैठने के लिए छटपटा रहे नेतागण चाहे जो वादे करते रहे हों या जो भाषण दें, वास्तविकता यही है कि बेरोजगारी और गरीबी को लेकर सरकारें गम्भीर नहीं रहीं। आजादी 1947 में मिली। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 से शुरू हुई। पर 1970 के बाद औपचारिक रूप से सरकारों के लिए यह ‘संभव’ हुआ कि वे गरीबी को परिभाषित कर सकें। गरीबी रेखा ‘खींच’ सकें। यह बता सकें कि भोजन के आधार पर, देहाती क्षेत्रों में 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का फार्मूला है। इससे नीचे का उपभोग करने वाला गरीबी रेखा के अंतर्गत है। 1974-1979 के आस पास ही कहीं न कहीं वे यह मानने को विवश हुए कि मात्र ‘विकास’ के परिणामस्वरूप बेरोजगारी कम नहीं होगी और न ही गरीबी कम होगी। और अब जाकर तथाकथित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी गरीबों के केवल पेट भरने के ही इर्द गिर्द थे और हैं- अभी भी। दूसरी तरफ पूंजीपतियों के तबके में कितनी तरक्की हुयी। देश के पूंजीपतियों ने कितनी प्रगति की- यह सभी को अच्छी तरह पता है। इसके अतिरिक्त और हो भी क्या सकता था- पूरी व्यवस्था उनकी है और उन्हीं के लिए है। देश के बेरोजगारों और गरीबों को कुछ राहत पाने के लिए किसी नयी व्यवस्था के बारे में सोचना-समझना और आगे बढ़ना होगा।